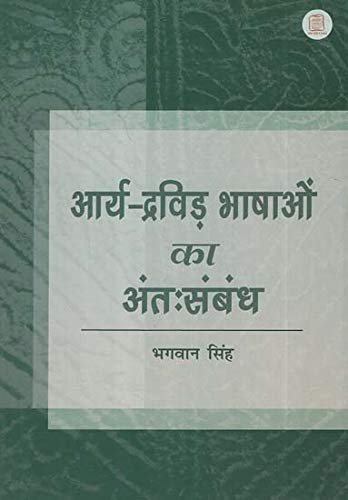
You May Also Like
The Balti a Scheduled Tribe of Jammu and Kashmir
- ByNanhi Shop
- February 17, 2025
Traditionally, the Baltis are believed to be descendants of Celtic communities settled in Scandinavia. When the water level…
The Mill on The Floss
- ByNanhi Shop
- September 10, 2024
The Mill on the Floss is a novel by George Eliot, first published in three volumes in 1860…
Issues and Concerns in Elementary Education
- ByNanhi Shop
- May 18, 2024
This Book is Dedicated to all the Teachers, Academicians, Researchers and Policy Makers who are working in the…
Women in Politics
- ByNanhi Shop
- April 19, 2025
These books are, Casteism in Indian Politics, published by Anmol Publications, New Delhi, Women Empowerment, published by Discovery…
Military History of India
- ByNanhi Shop
- February 6, 2024
This book is about wars fought in India from Alexander invasion to Mughal and Maratha period by a…
Relativity: The Special and General Theory
- ByNanhi Shop
- February 14, 2024
Relativity: The Special and General Theory, is an exact complete understanding of the theory of Relativity. It is…
